| schema:text
| - Last Updated on मार्च 21, 2024 by Neelam Singh
सारांश
एक सोशल मीडिआ पोस्ट द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारत में 67 लाख बच्चे रोज भूखे रहते हैं। जब हमने इस पोस्ट का तथ्य जाँच किया तब पाया कि यह दावा ज्यादातर गलत है।
दावा
ट्विवटर (वर्तमान में X) पर अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारत में 67 लाख बच्चे रोज भूखे रहते हैं।
इस तरह के पोस्ट्स यहां और यहां भी मौजूद हैं।
तथ्य जाँच
क्या इस तरह की रिपोर्ट जारी हुई है?
हां। हाल ही में भारत और अन्य जगहों पर 6 से 23 महीने की उम्र के बच्चों पर एक अध्ययन किया गया और इसकी रिपोर्ट 12 फरवरी को हार्वर्ड अध्ययन, JAMA नेटवर्क ओपन में प्रकाशित की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 6.7 मिलियन (19.3%) बच्चे zero-food category में आते हैं। इसका मतलब है कि देश में 67 लाख बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में कोई दूध या खाना नहीं खाया है।
अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत zero-food category में दुनिया के 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है, जहां बहुत सारे बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। गिनी (Guinea) 21.8% और माली (Mali) 20.5% आंकड़े के साथ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। इन देशों की स्थिति भारत से भी बदतर है। ऐसा कहा जाता है कि यह समस्या पश्चिमी अफ़्रीका, मध्य अफ़्रीका और भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित है।
Zero-food category क्या होती है?
Lancet के अनुसार जब बच्चे ने पिछले 24 घंटों में पर्याप्त कैलोरी सामग्री वाला कोई भी भोजन नहीं खाया हो, यानी कि कोई भी ठोस/ अर्ध-ठोस/ नरम/ गूदेदार भोजन, शिशु फार्मूला या पाउडर या डिब्बाबंद या ताजे दूध का सेवन भी ना किया हो, उसे zero-food category में डाला जाता है। इसे सीधे तौर पर समझें, तो इसका मतलब है कि 24 घंटे तक 6 से 23 महीने के बच्चे ने अपने अंदर कोई आहार ना लिया हो।
30 मार्च, 2023 को जारी शोध बताते हैं कि भारत में zero-food category का प्रचलन 1993 में 20.0% से घटकर 2021 में 17.8% हो गया। इस समयावधि में छत्तीसगढ़, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में zero-food के प्रचलन में उच्च वृद्धि देखी गई, जबकि नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
2021 में उत्तर प्रदेश (27.4%), छत्तीसगढ़ (24.6%), झारखंड (21%), राजस्थान (19.8%) और असम (19.4%) zero-food के सबसे अधिक प्रचलन वाले राज्य थे। देखा जाए, तो 2021 तक भारत में zero-food बच्चों की अनुमानित संख्या 5,998,138 थी। कुल मिलाकर देखा जाए, तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुविधा प्राप्त समूहों में वंचित समूहों की तुलना में zero-food का प्रचलन कम था।
क्या भारत सरकार ने हालिया जारी रिपोर्ट का समर्थन किया है?
नहीं। PIB पर जारी जानकारी के अनुसार सरकार का कहना है कि भारत में तथाकथित zero-food category पर 12 फरवरी, 2024 को JAMA नेटवर्क पर प्रकाशित लेख फर्जी खबरों को सनसनीखेज बनाने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। इसके लिए निम्न तर्क दिए गए हैं:
- “zero food children” की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है और इस पद्धति में पारदर्शिता का अभाव है।
- JAMA द्वारा जारी लेख शिशुओं के लिए मां के दूध यानी के स्तनपान के महत्व को स्वीकार नहीं करता है।
- अध्ययन में देश भर के 13.9 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर मापे गए 8 करोड़ से अधिक बच्चों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उल्लेख नहीं किया गया है।
- PMMVY योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। वहीं दूसरे बच्चे (लड़की) होने पर उसके उचित स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 6,000 रु की आर्थिक सहायता दी जाती है।
क्या वाकई यह रिपोर्ट फर्जी है?
कहा नहीं जा सकता। पहले भी ऐसी कई रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं, जिसका केंद्र सरकार द्वारा खंडन किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2023 (Global Hunger Index- 2023) में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर था, जिसे सरकार ने गलत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था।
इस सूचकांक में यह भी कहा गया था कि भारत में बच्चों की कमज़ोरी की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाती है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) के 2022 संस्करण में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। यह इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है।
क्या कोई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट भारत के लिए चुनावी मुद्दा है?
संभवतः नहीं। हालांकि सरकार द्वारा जारी आंकड़ें इस रिपोर्ट को गलत इंगित करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका पता तो केवल तब ही लग सकता है, जब समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाए।
देखा जाए, तो लोकसभा चुनाव – 2024 को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी रिपोर्ट्स को साझा करना दर्शाता है कि इसमें विरोधी देशों का कोई स्वार्थ निहित हो सकता है और लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के पोस्ट्स साझा किये जा रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि मतदाता को उल्लिखित बातों को सामने रखते हुए, सही या गलत का चुनाव करना होगा।
वहीं कोई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट भारत के लिए चुनावी मुद्दा है या नहीं, इसका चयन तो अब जनता पर है इसलिए इस विषय में किसी निर्णय पर पहुंचना गलत होगा क्योंकि सरकार द्वारा इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है।
अतः इस तर्क और विभिन्न शोध पत्रों एवं सरकार द्वारा किए गए दावों को मद्देनजर रखते हुए, कहा जा सकता है कि यह दावा ज्यादातर गलत है। हमने पहले भी इस तरह के दावों का तथ्य जाँच किया है, जिसे आप यहां पढ़ सकते हैं।
|


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)



![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
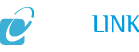

![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)